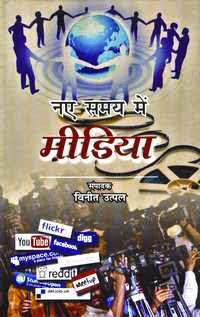पुस्तक 'सच कहता हूं’ हरीश चंन्द्र बर्णवाल की छह कहानी और 14 लघु कथाओं का
संग्रह है। पेशे से पत्रकार हरीश को इन कहानियों को लिखने में सोलह साल
लगे। शब्दों से खेलते हुए उन्होंने समसामयिक विषयों को भावनात्मक रूप से
अभिव्यक्त किया है।
वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आलोच्य पुस्तक की पहली
कहानी ‘यही मुंबई है’ अंधे बच्चों पर आधारित है। एक अंधे बच्चे को अपने ही
घर में, मां- बाप और भाई से दोयम दज्रे का व्यवहार मिलता है इसके बाद भी
उसकी यह सोच कि वह मुम्बई से अपनी मां के लिए दाई ढूंढकर ले आएगा, एक आदर्श
समाज की स्थापना का द्योतक है। बाल सुलभ बचकाना तर्क कि गुफाओं और सुरंगों
से होकर ट्रेन गुजरते समय आंख वालों को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता और यहां
अगर उसका भाई होता तो वह उसे भी कुछ समय के लिए अंधा कहकर चिढ़ा सकता था
जहां एक ओर उसकी शारीरिक विवशता बयां करती है वहीं दूसरी ओर उसके साथ किए
जाने वाले क्रूर बर्ताव की ओर भी इशारा करती है। कहानी रोचकता के साथ
मार्मिक कथ्य प्रस्तुत करती है। तभी तो वरिष्ठ लेखक राजेंद्र यादव लिखते
हैं कि कहानी की खूबसूरती यह है कि यह अपनी सीमा के पार चली जाती है.. जो
कथ्य है, जो कहा गया है, जो कहानी है, उसके पार ले जाती है और इसलिए यह
‘मेटाफर’ है। इस कहानी के लिए लेखक को अखिल भारतीय अमृतलाल नागर पुरस्कार
से नवाजा जा चुका है।
‘चौथा कंधा’ कहानी कादम्बिनी पुरस्कार से सम्मानित
है। इसमें गांवदे हातों में रहने वाले समाज में चल रही हलचलों को
तात्कालिकता में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे
किसी इंसान के मरने पर कोई हलचल पैदा नहीं होती जबकि ट्रेन से गाय कटने पर
कोहराम मच जाता है। लेखक ने परम्परावादी कथ्यों और प्रतिबिम्बों को कहानी
में बैसाखी नहीं बनाया है फिर भी देहाती समाज में नए के प्रति कौतुहल को
जिस शब्दजाल में पिरोया गया है, वह गुलजार का जुलाहा ही कर सकता है।
‘तैंतीस करोड़ लुटेरे देवता’ कहानी जम्मू के रघुनाथ मंदिर में घूमने के
दौरान के अनुभवों को आधार बनाकर लिखी गयी है। कहानी के माध्यम से मंदिर को
सब्जी बाजार बना चुके पंडितों पर कड़ा प्रहार किया गया है। एक व्यक्ति
कितनी शिद्दत और श्रद्धा से धार्मिक स्थल पर जाने की योजनाएं बनाता है
लेकिन जब वहां पहुंचता है तो इष्टदेव से मिलाने के लिए बिचौलिये बने
पंडितों के व्यवहार से उसकी सारी श्रद्धा सिरे से काफूर हो जाती है। जब भी
कोई सुधी पाठक इसे पढ़ेंगे, उन्हें अपने आस-पास की घटनाएं जरूर याद आएंगी।
कहानी ‘अंग्रेज, ब्राह्मण और दलित’ के जरिये हिंदू समाज में व्याप्त
जातिवाद के दंश को दिखाने की कोशिश की गई है।
जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की
कहानी ‘उसने कहा था’ में पहली प्रेम कहानी होने के बावजूद रोमांस का,
फैंटेसी का बाहरी आवरण नहीं दिखता, वैसे ही बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे
पर हरीश ने ‘काश मेरे साथ भी बलात्कार होता’ लिखी हैिबना किसी तरह के
अश्लील या भड़काऊ शब्द इस्तेमाल किए। आलोच्य संग्रह की यह सबसे संवेदनशील
कहानी कही जा सकती है। बलात्कार जैसे संवेदनशील मुद्दे को जिस साफगोई से
लेखक ने बाल चरित्रों के माध्यम से उठाया है, संभवत: इससे पहले किसी ने इसे
इस तरह नहीं उठाया होगा।
पुस्तक की आखिरी कहानी ‘अंतर्विरोध’ में भले ही
मुंबई के परिवेश और आधुनिक समाज की दिक्कतों को उकेरा गया है, लेकिन सभी
मेट्रो कल्चर के शहरों में यह परिवेश मिल जाएगा। इसमें दो पीढ़ी के बीच सोच
का अंतर ही नहीं, प्लास्टिक मनी के दौर में भी वस्तु विनियम पण्राली की
महत्ता को बरकरार दिखाया गया है। कहानी थोड़ी लम्बी है लेकिन जिन मुद्दों
को केंद्र में रखकर लिखी गई है, उसे देखकर छोटी ही महसूस होती है।
लघु
कथाओं में ‘बेड नं. छह’, ‘मेडिकल इंश्योरेंस’ के माध्यम से अस्पताल की
दिक्कत और ‘प्ले स्कूल’ और ‘बहाना’ में शिक्षकों की संवेदनहीनता को दर्शाया
गया है। ‘दो बड़ा या दो लाख’, ‘आखिरी चेहरा’, ‘गरीब तो बच जाएंगे ..’,
‘मायूसी’, ‘सिर्फ 40 मरे’, ‘बड़ी खबर’, ‘तीन गलती’, ‘कब मरेंगे पोप’ लघु
कथाओं में मीडिया में व्याप्त परेशानी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की त्रासदी
दिखाई देती है।
आलोच्य कहानियां जहां एक ओर मौजूदा समाज की सच्चाई का बखान
हैं वहीं दूसरी ओर पाठक को जीवन संघर्ष के प्रति प्रेरित भी करती हैं।
कहानी में दर्शाये गए पात्र पूर्वाचल के होने के बाद भी भाषाई स्तर पर
सुगठित दिखते हैं। कहानीकार अपनी कहानियों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को
समेटना चाहता है और एक हद तक इसमें सफल भी दिखता है। संग्रह का शीर्षक ‘सच
कहता हूं’ लेखक के मनोभाव को दर्शाता है जो संजय ग्रोवर की कविता या
मैं सच कहता हूं/ या फिर चुप रहता हूं/ ..बहुत नहीं तेरा लेकिन/ खुश हूं,
कम बहता हूं से प्रेरित लगता है।